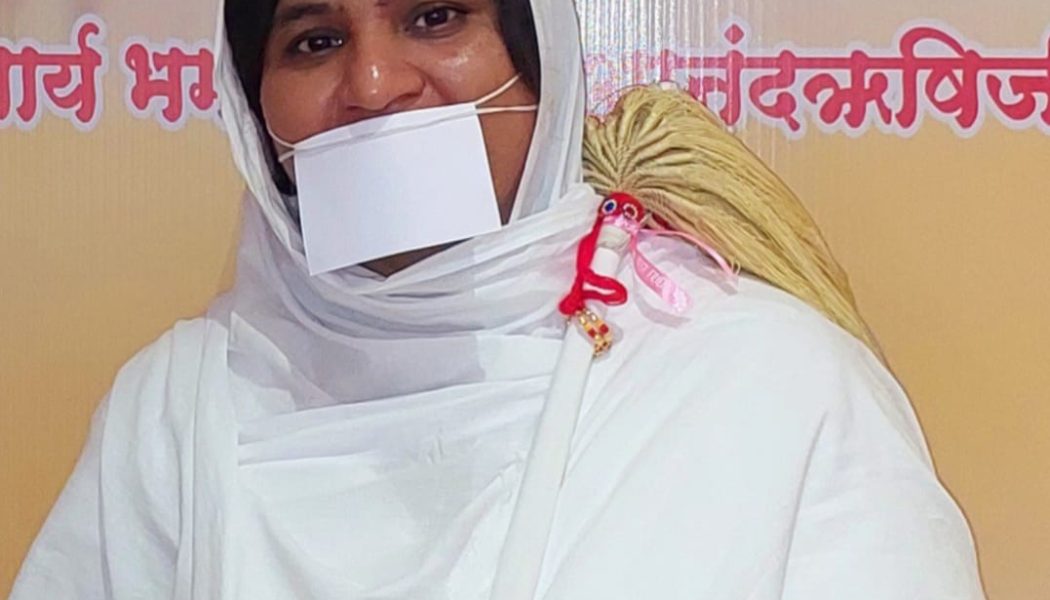हितकारी शुभ कार्यों में अरुचि रखना तथा धर्मक्रियाओं में अनुत्साह दिखाना प्रमाद है। प्रमादी मनुष्य का करणीय-अकरणीय का बोध धुंधला हो जाने से उसकी जागृति खो जाती है। प्रमाद का अर्थ मात्र आलस्य या नींद लेना ही नहीं है अपितु आत्मविस्मृति का नाम प्रमाद है। इसी कारण प्रमादी मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और नहीं करने योग्य कार्य में रुचि दिखाता है।
प्रभु महावीर ने समस्त दुःखों का मूल कारण प्रमाद को बताया है। जितने भी कर्मबन्ध होते हैं वे चाहे किसी भी माध्यम से हुए हों किन्तु उनके मूल में प्रमाद है। उच्च कोटि के साधक भी कभी अपरिहार्य कारण से तो कभी अकारण ही प्रमाद का सेवन करके अपनी आत्म-विकास की साधना को अवरुद्ध कर लेता है। प्रमाद तो एक प्रकार से जीते जी मृत्यु है।
गणधर गौतम स्वामी जैसे महान् साधक को भी प्रभु महावीर ने प्रमाद-त्याग की बार-बार प्रेरणा देते हुए कहा,
मनुष्य का जीवन वृक्ष से टूटे हुए पीले पत्ते के समान नश्वर है जो कुश के अग्रभाग पर स्थित ओस बिन्दुवत् है। इस अल्पकालिक जीवन में भी नाना प्रकार के विघ्न हैं। अतः कुशल साधक को क्षण भर के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए।
जहां प्रमाद है वहाँ विचार वाणी व व्यवहार में स्वच्छंदता होने से मनुष्य इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ में द्वेष करता है। वह अपना अमूल्य समय व्यर्थ की बातों को पढ़ने-सुनने में व्यतीत कर निरर्थक कर्मबन्ध कर लेता है ऐसे में आत्मशक्ति का दुरुपयोग होने से आत्म विस्मृति हो जाती है। अतः प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जन्म, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, धर्म-श्रवण व धर्मश्रद्धा का सुयोग मिलने पर साधक को सतत धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए।